राजनीति का दुर्लभ क्षण
राज्यसभा में दुर्लभ आम सहमति के साथ जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के साथ ही एक बड़े और बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधार का रास्ता साफ हो गया।
राज्यसभा में दुर्लभ आम सहमति के साथ वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के साथ ही एक बड़े और बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधार का रास्ता साफ हो गया। इस विधेयक को लेकर जिस तरह सभी दलों ने जैसी गंभीरता प्रदर्शित की उससे उच्च सदन की गरिमा बढ़ी और यह सुखद अहसास भी हुआ कि वे दलगत हित त्यागकर एकमत भी हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठा कि आखिर संघीय ढांचे या फिर राज्यों के अधिकार की आड़ लेकर संकीर्ण राजनीति क्यों की जाती रहती है? एक अन्य सवाल यह भी कि संसद भी इस राजनीति की चपेट में क्यों आ जाती है? इन सवालों के बीच जीएसटी संबंधी विधेयक का पारित होना एक लंबी कवायद का एक अहम पड़ाव भर है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी, लेकिन आम सहमति बनाने के लिए राज्यसभा में इसे संशोधन के साथ लाया गया। अब संशोधित विधेयक को दोबारा लोकसभा से पारित कराया जाएगा। इसके बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं को इसे पारित करना होगा और फिर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे।
वित्तमंत्री ने जीएसटी पर अमल के लिए एक अप्रैल 2017 की तारीख तय की है और उम्मीद की जा रही है कि समय कम होने के बावजूद इस बार यह समय सीमा आगे खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद कुछ अड़चनें अभी भी कायम हैं, जैसे जीएसटी की मानक दर क्या होगी और विवादों के निपटारे के लिए बनने वाला तंत्र किस तरह कार्य करेगा? कांग्रेस पहले जीएसटी की दर को संविधान संशोधन विधेयक का हिस्सा बनाए जाने पर जोर दे रही थी। बाद में जब वह इस मांग से पीछे हटी तो सरकार ने उसकी अन्य मांगों पर लचीला रुख अपनाया। अब उचित यही होगा कि दोनों पक्ष दर के निर्धारण का फैसला जीएसटी काउंसिल पर छोड़ दें। चूंकि फिलहाल एल्कोहल और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला हुआ है इसलिए आसार इसी बात के हैं कि जीएसटी के अमल में कोई गतिरोध नहीं पैदा होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह कोई बड़ा मसला नहीं कि जीएसटी से संबंधित सीएसटी और आइएसटी विधेयकों को मनी बिल के रूप में लाया जाए या नहीं? जीएसटी के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूरे देश में एक समान कर का विचार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के समय आया था। तब टैक्स सुधार संबंधी केलकर समिति ने इस तरह की व्यवस्था का सुझाव दिया था। संप्रग-एक सरकार में यह विचार लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रहा और बाद में वह राजनीतिक मुद्दा बन गया। ऐसा तब हुआ जब यह स्पष्ट था कि जीएसटी के अमल से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में एक से डेढ़ प्रतिशत की स्वत: वृद्धि हो जाएगी और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे।
जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों के करीब डेढ़ दर्जन अलग-अलग करों का स्थान लेगा और पूरे भारत को एक बाजार में तब्दील कर देगा। केवल एक टैक्स के साथ देश भर में वस्तुओं की आवाजाही से टैक्स संबंधी तमाम विवाद भी खत्म होंगे और उद्योग-व्यापार जगत की उलझनें भी। वित्तमंत्री ने राज्यों को आश्वस्त किया है कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाले नुकसान की पांच साल तक भरपाई केंद्र सरकार करेगी। दरअसल राज्यों को यह चिंता सता रही है कि वैट और चुंगी सरीखे तमाम टैक्स समाप्त हो जाने से उनका राजस्व घट जाएगा और स्थानीय निकायों को अपने राजस्व के लिए अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी। चूंकि वस्तुओं पर औसत टैक्स की दर 25 प्रतिशत के आसपास रहती है इसलिए शुरुआती वर्षों में कुछ नुकसान होना तय है, फिर भी जीएसटी दर को बहुत ऊंचा नहीं रखा जा सकता। ऊंची दरें उद्योगपतियों और व्यापारियों को टैक्स चोरी के लिए प्रेरित करती हैं। अगर ऐसा हुआ तो जीएसटी का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा। जीएसटी दर ऐसी हो कि व्यापारी टैक्स भरने के लिए प्रेरित हों। इससे न सिर्फ काले धन के कारोबार पर अंकुश लगेगा, बल्कि टैक्स का दायरा भी बढ़ेगा। इसके साथ ही औद्योगिक-व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा। स्पष्ट है कि इस सबका लाभ आम जनता को भी मिलेगा। एक ही देश में केंद्र और राज्यों के स्तर पर तमाम तरह के टैक्स का होना प्रशासनिक अकुशलता का ही नमूना है। इस खामी को करीब डेढ़ दशक पहले ही भांप लिया गया था, लेकिन आश्चर्य है कि उसे दूर करने में इतना लंबा वक्त लग गया। इस देरी की सबसे बड़ी वजह सुधार की पहल पर संकीर्ण राजनीति रही।
यह अजीब है कि हमारे राजनीतिक दल एक ऐसे सुधार पर सहमति कायम नहीं कर सके जिसे लगभग पूरी दुनिया ने अपना लिया है। भारत ने जब जीएसटी के बारे में सोचा था तब इस तरह की व्यवस्था केवल 34 देशों में थी, लेकिन आज करीब 160 देश एकल टैक्स की व्यवस्था को अपना चुके हैं। इससे पता चलता है कि एक महत्वपूर्ण सुधार अपनाने में भारत कितना पीछे रह गया। वैसे तो दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस इस महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के पक्षधर थे, लेकिन कभी अहं और कभी श्रेय के चक्कर में वे एक-दूसरे को सहयोग देने से बचते रहे। ये दोनों दल भी यदा-कदा क्षेत्रीय दलों की तरह संघीय ढांचे का हवाला देते दिखे। देशहित की अनदेखी कर संघीय ढांचे के खतरे की आड़ लेना राजनीतिक संकीर्णता के अलावा और कुछ नहीं। आजादी के इन 70 वर्षों में यह साबित हो चुका है कि भारत का संघीय ढांचा बेहद सशक्त है और बात-बात पर इस ढांचे के अस्तित्व अथवा राज्यों की स्वायत्तता के समक्ष खतरे की आशंका संकीर्ण राजनीति है। बावजूद इसके अक्सर राजनीतिक दलों की ओर से ऐसे काल्पनिक खतरे खड़े किए जाते रहते हैं। इससे देशहित की अनदेखी होती है। विडंबना यह है कि राजनीतिक दल तब संघीय ढांचे की परवाह करते नहीं दिखते जब उन्हें राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन करना होता है। वे मुख्यमंत्रियों तक को यकायक बदल देते हैं या फिर व्यवस्था और संस्थाओं को मजबूत बनाने वाले कदमों को अपनाने से इंकार कर देते हैं। पुलिस सुधारों की अनदेखी इसका उदाहरण है। राजनीतिक दलों के प्रभाव क्षेत्र वाले राज्यों की आम जनता से पूछा जाए तो वह सदैव राष्ट्रीय महत्व के मसलों को प्राथमिकता देना पसंद करेगी, लेकिन ऐसे दल क्षेत्र-राज्य के हितों के नाम पर संकीर्ण राजनीति करते ही रहते हैं।
यह राजनीतिक दलों की संकीर्णता ही कही जाएगी कि जीएसटी पर आम सहमति बनाने में उन्हें करीब एक दशक लग गया। यह ठीक है कि जीएसटी पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष ने दलगत हितों से ऊपर उठकर संजीदगी दिखाई और सार्थक बहस भी की, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी संजीदगी और ऐसी धीर-गंभीर चर्चा दुर्लभ क्यों? क्या राजनीतिक दलों का प्राथमिक दायित्व यही नहीं कि वे प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर व्यापक चर्चा करें और देश को दिशा दें? अच्छा हो कि सभी दल अपने मूल दायित्व को न केवल पहचानें, बल्कि उसे प्राथमिकता भी प्रदान करें। इससे ही देश उन समस्याओं से मुक्त होगा जिनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक हो चुका है। यह ठीक नहीं कि जब राजनीतिक दलों को सुधारों की पहल करते दिखना चाहिए तब वे उस पर अड़ंगा लगाते अथवा संकीर्णता का प्रदर्शन करते या फिर संघीय ढांचे को खतरे का बेजा सवाल उठाते अधिक दिखते हैं।
[ लेखक संजय गुप्त, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं ]




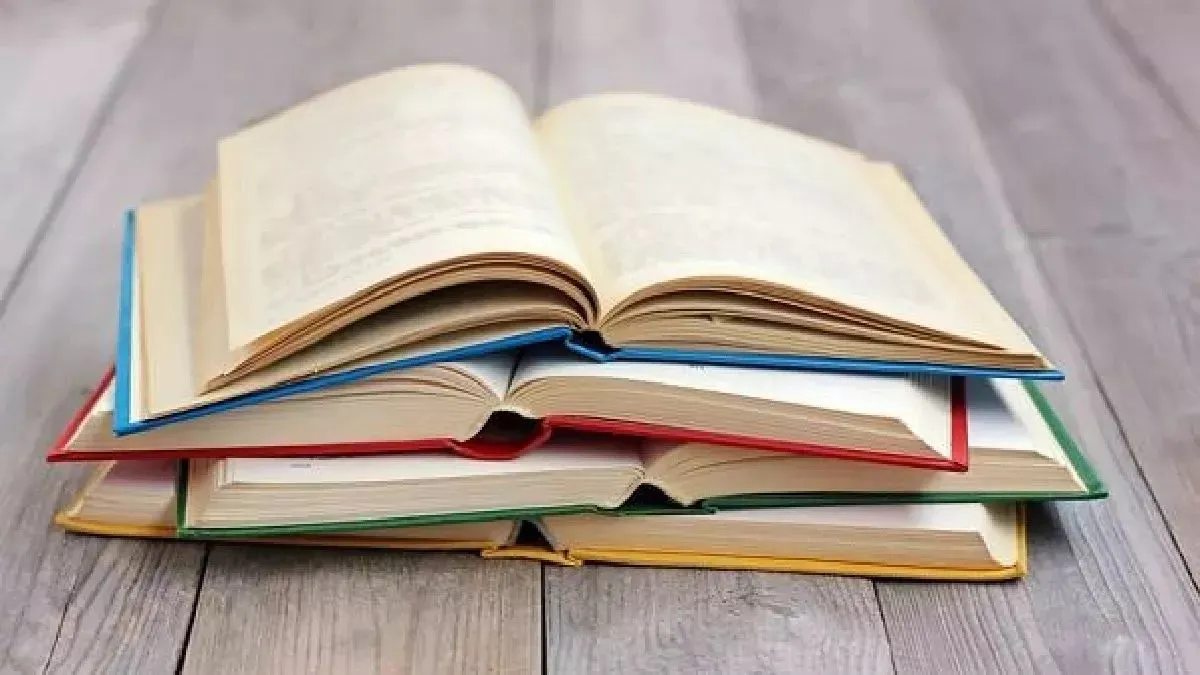









कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।