हिंदी के प्रति संकीर्ण सोच
अंग्रेजी भाषा कितनी महान है। वहां कुछ भी छिपाया नहीं जाता और हिंदी वाले कितने पिछड़े हुए हैं कि वे खुद से और विशेषकर अपने बच्चों से सब कुछ छिपा लेना चाहते हैं।
अवसर था एक साहित्यिक आयोजन का। इसमें तीन युवा साहित्यकार थे। दो स्त्रियां और एक पुरुष। तीनों ही अंग्रेजी के लेखक। पहली लेखिका ने शिकायत की कि उन्हें अपनी किताबों का हिंदी अनुवाद कराते हुए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी किताबों में लिखे हुए शब्दों का जब हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की जाती है तो जो शब्द मिलते हैं उन्हें छापने में प्रकाशक भी आनाकानी करने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर ये शब्द छापे तो कहीं विरोध प्रदर्शन न होने लगें, कहीं कोई किताबों को जलाने न लगे। लोग अपने प्राइवेट पार्टस का नाम लेने से भी हिचकते हैं और उनकी जगह कुछ और बोलते हैं। दूसरी लेखिका ने कहा कि मैंने अपने ड्राइवर को अपनी हिंदी में अनुवादित किताब दी तो उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मेरे पति से शिकायत की कि हिंदी में अच्छा अनुवाद नहीं है। बड़े-बड़े गंदे शब्द लिखे हैं। तीसरे पुरुष लेखक ने कहा कि हम अकसर बहुत कुछ छिपा लेना चाहते हैं, खास तौर से अपने बच्चों से। इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जब उनका सातवां जन्मदिन मनाया गया तो उनके मन में विचार आया कि आखिर वह इस दुनिया में आए कैसे। इस बारे में अपनी मम्मी से पूछा तो वह बोलीं कि वह मुझे दुकान से उठाकर लाई थीं। पिताजी ने कहा कि गुरुद्वारे से लाए थे। तभी मैं समझ गया कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। जब मैं ये सब बातें समझने लायक हुआ तो मुझे लगा कि आखिर हम इतना छिपाते क्यों हैं? हम अपने माता-पिता को इस रूप में देखना ही नहीं चाहते हैं कि उन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा।
इन तीनों की बातें सुनकर लगा जैसे कि इनकी मंशा यह बताने की हो कि देखिए अंग्रेजी भाषा कितनी महान है। वहां कुछ भी छिपाया नहीं जाता और हिंदी वाले कितने पिछड़े हुए हैं कि वे खुद से और विशेषकर अपने बच्चों से सब कुछ छिपा लेना चाहते हैं। दरअसल मुश्किल ही यह है कि प्रगतिशील होने और दिखने के लिए यह जरूरी है कि हिंदी में दो लात लगाते हुए हिंदी के लोगों को कुछ ज्ञान दिया जाए। इसमें अंग्रेजी लाठी बड़ी कारगर होती है, क्योंकि प्रगतिशील विचारों का आखिरी खूंटा और ठेका सिर्फ पश्चिम और अंग्रेजी के पास है। इन अंग्रेजी वालों को हिंदी में आना है, क्योंकि असलियत में ये जानते हैं कि गोरी चमड़ी वालों की अकड़ के आगे ये कहीं नहीं टिकते। हां हिंदी में आते ही रातोंरात इन्हें सितारों की तरह चमका दिया जाता है।हिंदी का बड़ा समाज, बड़ा पाठक वर्ग, बड़ा सर्कुलेशन, बड़ा नाम, बड़ी रायल्टी और उसके बदले मिलते बड़े इनाम और फेलोशिप तो चाहिए मगर ये जताते हुए कि देखो हिंदी में आकर हमने कितना अहसान किया। हिंदी के लोगों को हमारा कृतज्ञ होना चाहिए। इनकी बातें सुनकर लगा कि संसार में लव, लस्ट और सेक्स के अलावा मनुष्य की और कोई समस्या है ही नहीं। और हिंदी वाले तब ही प्रगतिशील कहे जा सकते हैं जब वे बच्चों को जन्मते ही इस बारे में बताने लगें। छिपाने की भी एक खूबसूरती होती है, साहित्य में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का भी कोई स्थान है, इसे ये जानते तक नहीं। पढ़ा हो तो जानें। इसके अलावा सही उम्र में हर कोई सब कुछ सीख ही जाता है, उसे इनकी रचना पढ़कर स्त्री-पुरुष संबंधों की बारीकियां जानने की जरूरत शायद ही पड़ती हो। सेक्स के बारे में बताने का एक बड़ा तर्क पश्चिमी चश्मे वाले यह भी देते हैं कि इससे बच्चों को यौन अपराधों से बचाया जा सकता है। लेकिन जिन देशों में प्राथमिक स्तर से ही बच्चों और विशेषकर बच्चियों को इन बातों के बारे में बताया जाता है, क्या वहां यौन अपराध रुक गए हैं। जी नहीं, बल्कि बहुत से देशों की आबादी के लिहाज से उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। यही नहीं किशोरावस्था में गर्भधारण एक बड़ी समस्या है। दस-बारह साल के बच्चे तक मां-बाप बन जाते हैं। इसके बावजूद कि अधिकांश स्कूलों में वे मशीनें लगी हुई हैं जिनसे गर्भनिरोधक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि बच्चों को ऐसा ही जीवन देना आदर्श है जहां वे पढ़ाई-लिखाई और खेल छोड़कर बचपन से ही उन बातों में लग जाएं जिनकी उनकी उम्र नहीं है। यदि हिंदी क्षेत्र में बच्चों को उम्र से पहले इन बातों को नहीं बताया जाता तो भाई तकलीफ क्या है? और अगर तकलीफ है तो अपने आसपास, परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें सब बता दो, किसने रोका है। बहुत साल पहले फैंटेसी पत्रिका के संपादक ने कहा था कि वह अपनी पत्रिका घर नहीं ले जाते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे उसे देखें। शायद अंग्रेजी विचार और उसे हर हालत में सही साबित करने वाला चश्मा ऐसा ही करता है। इसमें अपने बच्चों को वह सब नहीं दिखाना है, जिसे आप दूसरों के बच्चों को दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं? जिससे कि आपकी पत्रिका के ग्राहक बचपन से ही बन जाएं। और हिंदी में पोर्न का एक फलता-फूलता बाजार बना दिया जाए, जिसके पाठक-दर्शक बच्चे हों। क्या इसी तरह बच्चों को यौन अपराधों से मुक्ति मिल सकती है?
आजकल हॉलीवुड और वॉलीवुड से सीखकर यह कुछ रिवाज सा भी चल पड़ा है कि कोई भी रचना चाहे वह फिल्म हो, उपन्यास, कहानी, नाटक हो, विज्ञापन हो, कविता हो, जब तक चर्चित न हो तब तक अच्छी नहीं मानी जा सकती और वह चर्चित कब होती है, जब उसमें चार-छह बेडरूम सीन, गाली-गलौज और जोरदार सेक्स का तड़का न हो। एक तरफ कहा जाता है कि भारत में तो कामसूत्र रहा है। खजुराहो के मंदिर हैं, फिर यहां इतनी रोक-टोक क्यों है। लेकिन कामसूत्र का नाम लेने वाले यह भूल जाते हैं कि उसमें कुछ मर्यादाओं का जिक्र भी है और सबसे बड़ी मर्यादा उम्र की है। मगर जैसे ही कोई मर्यादा की बात करेगा, उसे फौरन अंग्रेजी दिमाग प्रतिक्रियावादी, कंजरवेटिव, हिंदूवादी, पिछड़ा आदि महान बातों से सुशोभित कर देंगे। अक्सर ऐसे उत्सवों में रणनीति के तहत कोई न कोई ऐसा मुद्दा गरमाया जाता है जिससे चस्केदार विवाद हो और उत्सव अधिक से अधिक चर्चा में आए।
[ लेखिका क्षमा शर्मा, साहित्यकार और स्तंभकार हैं ]




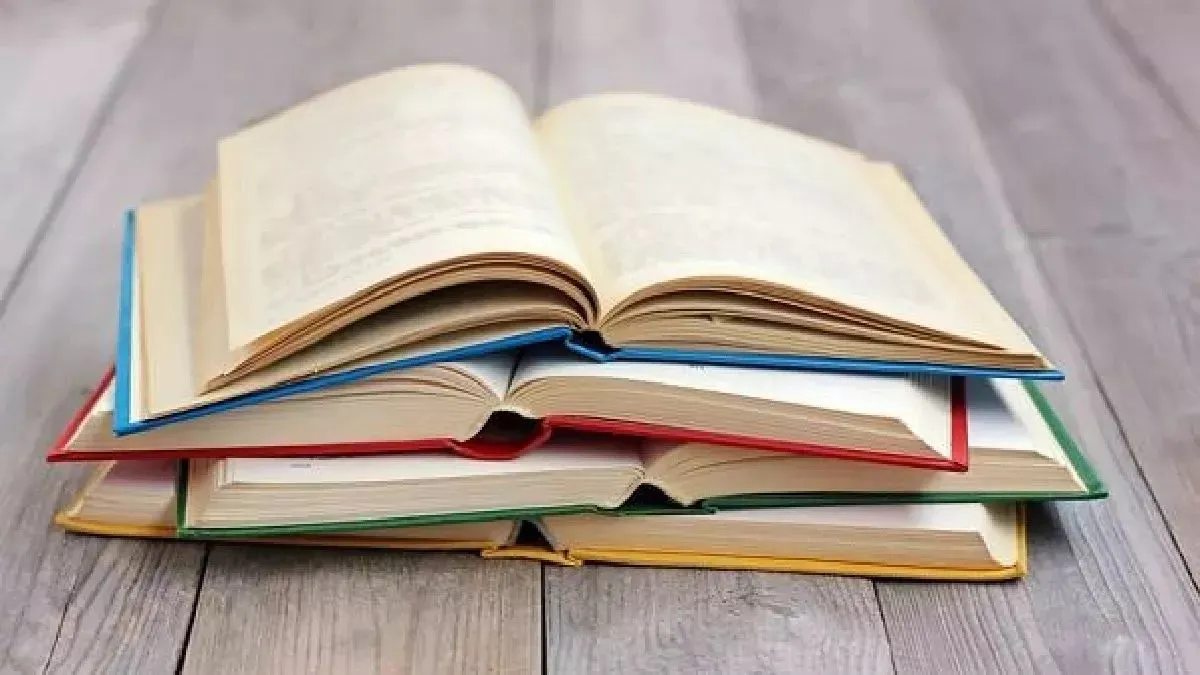









कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।