दूरगामी नुकसान करते लुभावने वादे, बढ़ जाती है वित्तीय अस्थिरता और आर्थिक संकट की आशंका
वास्तविकता यही है कि इस लोकलुभावनवाद ने चुनावी वादों और आर्थिक व्यावहार्यता के बीच तनाव की स्थिति बना दी है जिसके सामाजिक कल्याण एवं स्थायित्व पर दूरगामी प्रभाव दिख सकते हैं। लोकलुभावनवाद के मुद्दे पर मंथन के लिए हमें दो बुनियादी पहलुओं की पड़ताल करनी होगी।
विवेक देवराय आदित्य सिन्हा: समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में लोकलुभावनवाद का ही बोलबाला दिख रहा है। कई देशों के अलावा भारतीय राजनीति को भी यह पहलू प्रभावित कर रहा है। सत्ता की चाह में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाते हैं। हालांकि, सत्ता में आते ही वित्तीय बाधाओं के चलते ये वादे खोखले साबित होते हैं। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी नुकसान वाले ये वादे वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे लेकर चिंता प्रकट करते हुए राज्य सरकारों से यही कहा कि वे वित्तीय अनुशासन के दायरे में ही जनकल्याण करें।
प्रधानमंत्री मोदी या अन्य लोगों की ऐसी चिंता अकारण भी नहीं। राजनीति में मुफ्त उपहारों की यह रेवड़ी संस्कृति धीरे-धीरे अपनी पैठ गहरी करती जा रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। वहां कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों ने अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न कर दी है। मुफ्त बिजली और बस यात्रा जैसे वादे कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुए। यही कारण है कि तमाम लोगों ने अब बिजली के बिल भरना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस वादे को पूरा करेगी और उन्हें मुफ्त बस यात्रा की सौगात भी मिलेगी।
वास्तविकता यही है कि इस लोकलुभावनवाद ने चुनावी वादों और आर्थिक व्यावहार्यता के बीच तनाव की स्थिति बना दी है, जिसके सामाजिक कल्याण एवं स्थायित्व पर दूरगामी प्रभाव दिख सकते हैं। लोकलुभावनवाद के मुद्दे पर मंथन के लिए हमें दो बुनियादी पहलुओं की पड़ताल करनी होगी। पहला यही कि आखिर लोकलुभावनवाद क्या है? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह ऐसी रणनीति प्रतीत होती है, जिसमें तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति वाले वादों को जनता के बीच व्यापक समर्थन मिलता है। हालांकि, आरंभिक स्तर पर लोकप्रियता के बावजूद दीर्घकालिक स्तर पर इनके व्यापक दुष्प्रभाव होते हैं। इनसे न केवल अन्य आवश्यक खर्चों के लिए संसाधनों की कमी पड़ती है, बल्कि वित्तीय स्थिति भी बिगड़ती है।
दूसरा पहलू यही कि यदि लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है तो फिर लोकलुभावनवाद में क्या समस्या है? नि:संदेह, लोकलुभावनवाद में जनता की इच्छा प्रतिनिध्वनित होती है और यही लोकतंत्र का मूल अधिकार भी है, लेकिन सवाल यही है कि इनके समीकरणों में मूलभूत समस्याएं हैं। लोकलुभावन प्रवृत्तियों के चलते पार्टियां बड़े-बड़े वादे करती हैं और उस हिसाब से उनकी पूर्ति नहीं कर पातीं तो जनता का भरोसा घटता है। इन सबसे बढ़कर लोकलुभावन नीतियों से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी होती है।
इनसे कुछ तात्कालिक लाभ भले ही मिल जाएं, लेकिन बजटीय घाटे, वित्तीय अस्थिरता और अंतत: किसी आर्थिक संकट की आशंका बढ़ जाती है। इससे जुड़ा विमर्श अक्सर सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है तो सामाजिक सद्भाव और एकता की भावना पर आघात करता है। इससे सतत विकास और नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस कारण कई लचर नीतियां अस्तित्व में आ जाती हैं। भले ही लोकलुभावनवाद को आम आदमी के हितों की पैरवी करने वाला बताया जाता हो, लेकिन यह सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को उलटकर असमानता एवं अन्याय को बढ़ावा दे सकता है।
ऐसे में यह युवा मतदाताओं का दायित्व है कि वे लोकलुभावनवाद के संभावित दुष्प्रभावों को समझते हुए इस पर विराम लगाने के लिए आगे आएं, क्योंकि यह उनके भविष्य का प्रश्न है, जिसमें आर्थिक संतुलन को असंतुलित करने का जोखिम है। पंजाब का उदाहरण लें तो उसके बजट की पड़ताल कई चिंतित करने वाले रुझान दर्शाती है। राज्य की जीडीपी के अनुपात में कर संग्रह खतरे की घंटी बजाने वाला है।
इससे केंद्रीय वित्तीय सहायता पर राज्य की निर्भरता बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में पंजाब पर 3,12,758 करोड़ रुपये का कर्ज दिखाया गया, जिसके अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 3,27,050 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाने के आसार हैं। ये महज कुछ आंकड़े नहीं, बल्कि आर्थिक आपदा के संकेतक हैं। ऐसे में लोकलुभावन योजनाओं के नकारात्मक दूरगामी पहलुओं को देखते हुए उन्हें लेकर सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाना ही उचित है।
लोकलुभावनवाद के साथ एक बड़ी चिंता यही है कि इससे प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने की अंतहीन होड़ शुरू होगी। यह प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद समय के साथ चिंता बढ़ाता जाएगा। पेंशन योजना से लेकर मुफ्त बिजली तक इस सिलसिले पर कोई विराम नहीं लगेगा। हमारे जैसे विकासशील देश में जहां संसाधन सीमित हैं, वहां सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं बेतरतीब होने के बजाय रणनीतिक स्वरूप वाली एवं लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाना ही उचित है। अन्यथा संसाधनों के दुरुपयोग की चुनौती उत्पन्न होती है।
दिल्ली का ही उदाहरण लें, जहां 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। चार मंजिला बंगले की स्थिति में देखें तो वहां बिजली के चार अलग-अलग कनेक्शन संभव हैं। इससे वहां 1,600 यूनिट मुफ्त बिजली की संभावना बनी रहेगी। लोगों को इसकी इतनी आदत लग चुकी है कि जब दिल्ली सरकार ने इसे वैकल्पिक बनाया तो 58 लाख उपभोक्ताओं में से 48 लाख ने सब्सिडी के विकल्प को वरीयता दी।
ये उदाहरण हमें हमारी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को समझने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस दिशा में यह आवश्यक होगा कि सरकारी खर्च संसाधन संपन्न लोगों पर न होकर वास्तविक जरूरतमंदों पर होना चाहिए। यह मुद्दा संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने और असमानता को बढ़ने से रोकने से भी जुड़ा है। इन महत्वपूर्ण अंतरों को समझने पर ही हमारे राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है।
(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव-अनुसंधान हैं)




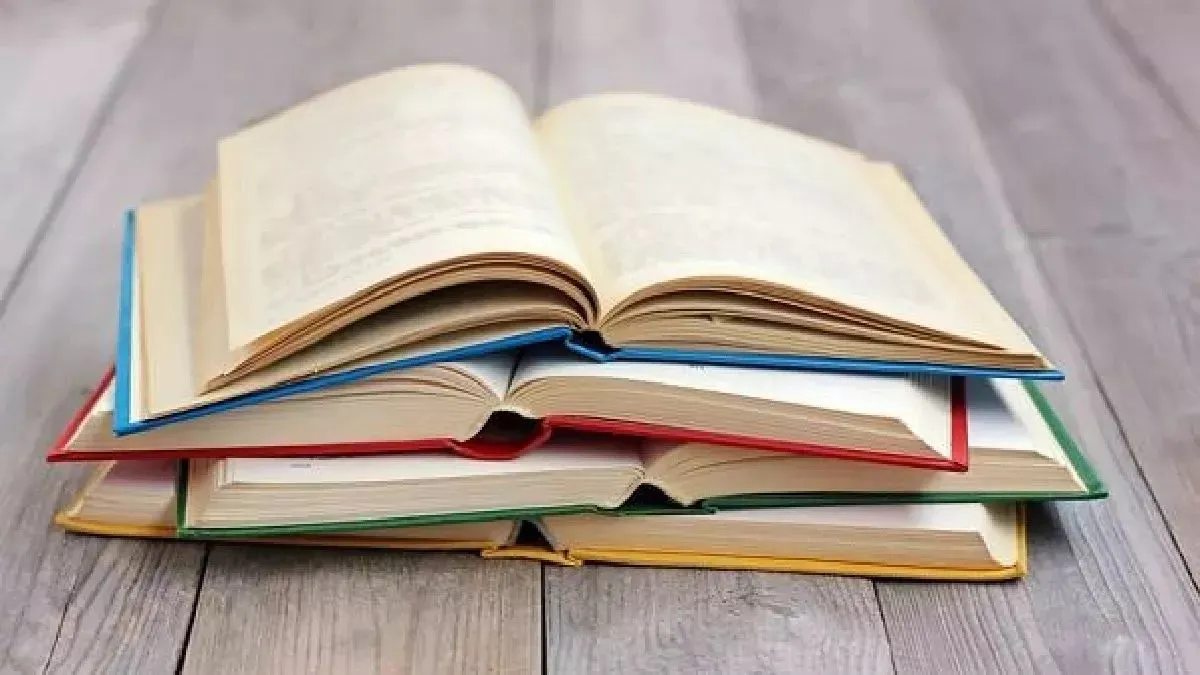









कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।