संसार और संन्यास
संन्यास संसार में रहते हुए भी उसे अपने में अनुभव न करने की स्थिति की मानसिक अवस्था का नाम है। संत या संन्यासी वही होता है जिसका मन बीतरागी हो चुका हो। रामकृष्ण गृहस्थ वेष में रहते हुए भी परमहंस कहलाए। आज भी संसार में मुक्त रूप से जीते हुए, हमारे आसपास, विरागी व्यक्तियों के अस्तित्व हैं, पर वेष के अभाव में, हम जैसे दिखने के कारण वे हमें संन्यासी नहीं लगते। वे चाहते भी नहीं कि लोग उन्हें संन्यासी, विरागी या संत समझें या उन्हें ऐसे असामान्य संबोधन से समादृत करें। वासनाओं से प्रदूषित समाज का असंतुलन ऐसे ही सामान्य दिखने वाले गृहस्थों के कारण ही बना हुआ है। ऐसे लोगों को हम साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं जो औरों का भला चाहते हैं। अपने किसी आचरण से औरों को दुख न पहुंचाएं। जो आत्मपोषी हो, सब में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता हो और दूसरे के धन, स्त्री, वैभव की अपने लिए कामना भी जिसके मन में न उठे वह किसी भी वेष में हो, किसी भी काया में हो, संन्यासी ही माना जाएगा। इसलिए हमें न तो वस्त्र रंगने की आवश्यकता है और न नाम या आश्रम बदलने की, अगर जरूरत है तो अपनी कामनाओं को सीमित करने की। कामना और वासना के दैत्यों से जूझने की स्थली का ही नाम संसार है। हमें परिस्थितियों से पलायन नहीं उनसे सामंजस्य स्थापित कर केवल अपना कर्म ही करने का अधिकार मिला है।
संसार में जो पाना है वह अपनों के बीच से ही पाना है। धर्म और कर्म का समन्वय ही योग है। कृष्ण अर्जुन से योगी होकर कर्म करने की बात करते हैं, फल पर दृष्टि रखने की नहीं। जो संन्यास लेते हैं वह यह संकेत देते हैं कि भौतिकता से परिपूर्ण संसार अब मात्र एक छोटे से वस्त्र के रूप में तन से लिपटा रह गया है। जो भी कर्म वे करते हैं वह समाज को परमात्मा का स्वरूप समझ उसके लिए करते हैं। त्याग उनकी वृत्ति होती है और मोक्ष उनका लक्ष्य। हम यह गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी कर सकते हैं।
[डॉ. जीवन श़ुक्ल]
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर









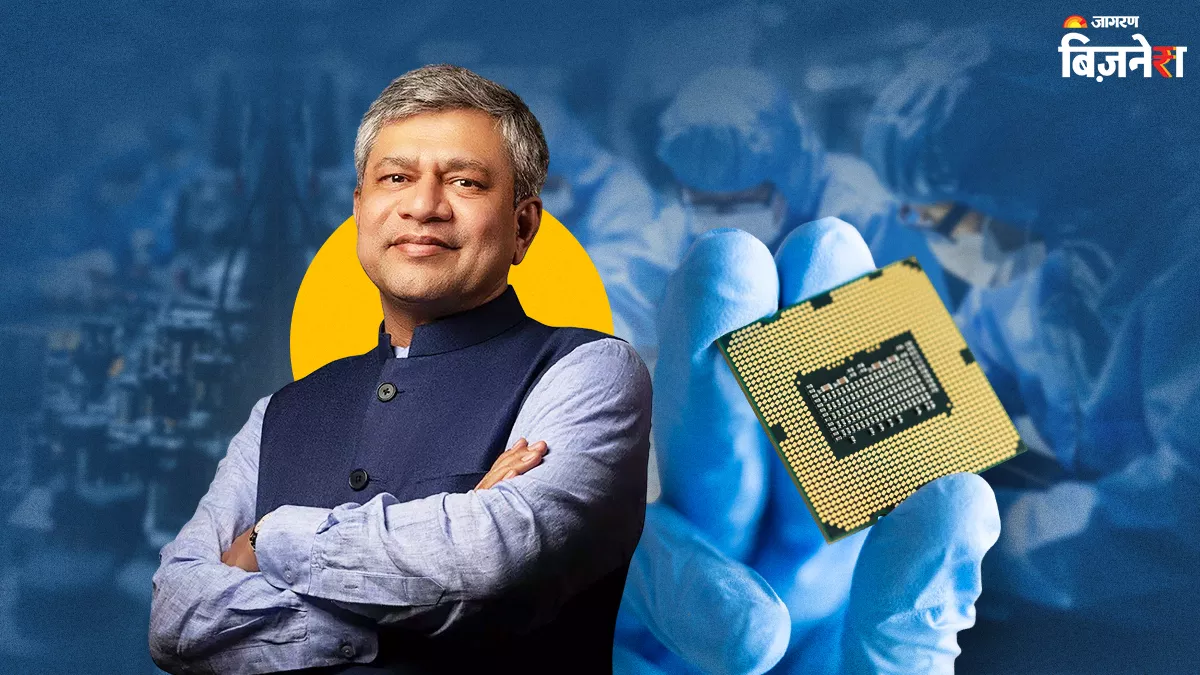


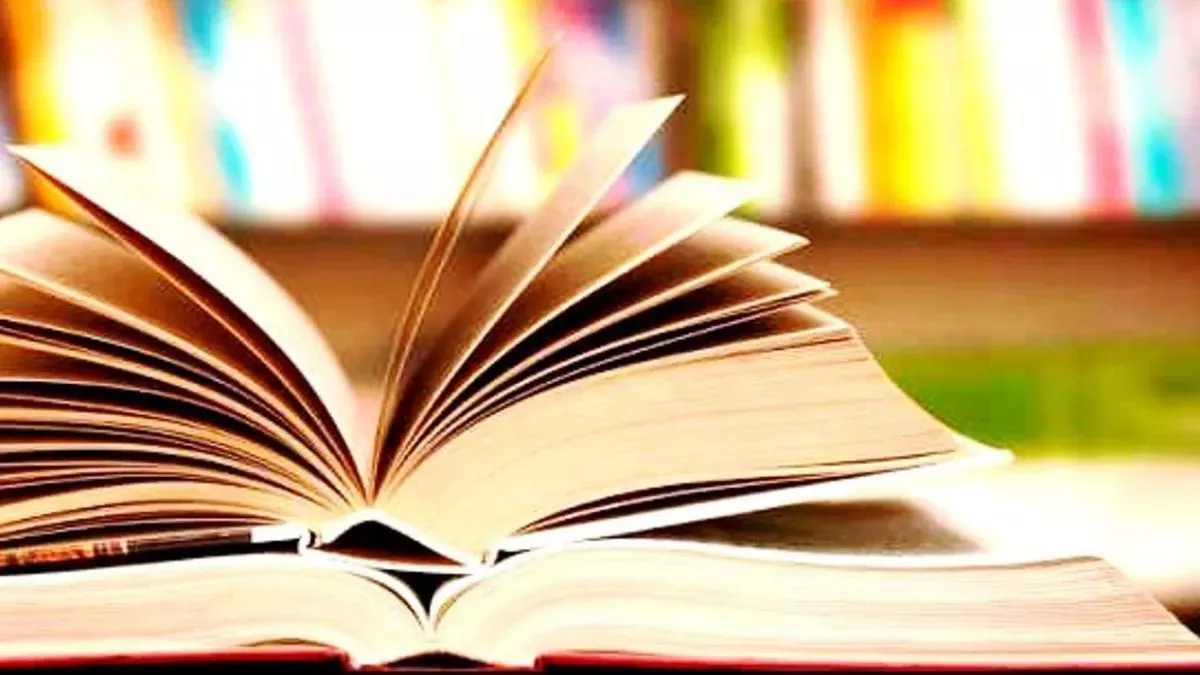

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।