विचार: सांसद अपनी भी समीक्षा करें, संसद की कार्यवाही चलाने की बजाय रोकने की कवायद तेज होने लगी
सरकार के लिए विधेयक अहम हैं। कई बार तो यह सुविधाजनक भी होता है कि अवरोध में ही विधेयक पारित करा लिए जाएं लेकिन सवाल विपक्ष का है कि वह सरकार के मुफीद ऐसा माहौल बनाता ही क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक बड़ा कारण होता है हर दो-तीन महीने में होने वाले चुनाव। ऐसे में सबको वही मुद्दे चाहिए जो गर्मी पैदा कर सकें।
आशुतोष झा। संविधान, लोकतंत्र तो कुछ अरसे से राजनीति में चर्चा के केंद्र में है ही, लेकिन वक्त आ गया है कि अब विधायिका पर भी चर्चा हो और इसका ठोस आकलन हो कि संसद जन आकांक्षाओं को पूरा कर पा रही है या नहीं? यदि नहीं तो इसके लिए उत्तरदायी कौन हैं, कितना हैं और क्यों हैं? संसद सही तरह से तब काम करेगी, जब पक्ष-विपक्षी के दल यानी सांसद अपना काम ठीक से करेंगे।
संसद के सदस्यों को कैसे जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र एजेंसी इसका पूरा अध्ययन कर जनता के सामने रख दे कि किसे जिम्मेदार माना जाए? संसदीय परंपरा, नियम-कानून की कसौटी पर यह अध्ययन हो और उसे सार्वजनिक किया जाए। यह इसलिए जरूरी हो गया है, क्योंकि साल दर साल संसद की कार्यवाही चलाने की बजाय रोकने की कवायद तेज होने लगी है।
बहस की गुणवत्ता के बजाय शोर के जोर से सफलता आंकी जाने लगी है। जनता के असल मुद्दों के बजाय आमतौर पर सतही राजनीतिक और चुनावी मुद्दे हावी होने लगे हैं। याद कीजिए कि किसी संसदीय सत्र से पहले ऐसी खबर पढ़ी क्या कि सत्र बहुत फलदायक होने वाला है...। यह खबर हर बार पढ़ी होगी कि हंगामेदार रहेगी। आरोप- प्रत्यारोप इस पर चलता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार विधेयक लेकर आती है। विपक्ष के पास पूरा अधिकार होता है कि उन पर अपने विचार रखे, लेकिन विपक्ष का एजेंडा तय करता है कि सदन की कार्यवाही चल पाएगी या नहीं?
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में थोड़ी भी रुचि रखने और दलगत राजनीतिक हित से अधिक देश की चिंता करने वाले किसी जागरूक नागरिक से यदि पूछा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत-पाक सैन्य टकराव रुकवाने का जो दावा किया गया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार का क्या कहना है? जवाब यही आएगा कि प्रधानमंत्री ने उस दावे को कड़ाई से तब खारिज कर दिया था, जब वह कनाडा गए थे और वहां से ट्रंप पर फोन से बात की थी। आपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों में गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल में सब दलों के सांसदों ने वैश्विक मंच पर क्या कहा, सबको पता है। इन प्रतिनिधिमंडलों में कांग्रेस के भी कई सांसद थे।
आखिर संसद में विपक्ष क्या जानना चाहता है? ट्रंप के बड़बोलेपन से दुनिया परेशान है। जिन देशों के साथ वह व्यापार समझौते की घोषणा कर रहे हैं, वे अचंभित हैं, लेकिन हमारे तमाम विपक्षी सांसद हैं कि उन्हें ट्रंप के बडबोले बयानों और बेतुके दावों पर चर्चा करनी है। आपरेशन सिंदूर में सेना की वीरता पर देश का सीना गर्व से चौड़ा है। संसद में बहस करना चाहें तो कर लें, लेकिन क्या सेना की रणनीति पर चर्चा करेंगे या सेना को यह बताने की कोशिश करेंगे कि सैन्य रणनीति कैसे बनाई जाती है? ऐसे मुद्दों पर संसदीय स्थायी समिति में खुलकर बात हो सकती है, लेकिन जोर सदन में चर्चा का है।
बिहार में चुनाव आयोग की और से चल रहा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पहली सुनवाई में कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया और संभवतः अगले सप्ताह फैसला आ सकता है। फिर चर्चा किस चीज पर? फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार को माना है और केवल समय को लेकर और नागरिकता तय करने के संदर्भ में सवाल उठाया है। आखिर हर संसद सत्र में घड़ी की सुई को पीछे लाने की कोशिश क्यों होती है? सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन उस चर्चा का सार्थक होना भी जरूरी है, खासकर तब जब संसद साल में बमुश्किल 40-50 दिन ही सुचारू हो पाती है।
राजनीतिक दलों की ओर से मांग की जाती रही है कि साल में कम से कम सौ दिन सत्र चलना चाहिए, लेकिन अब इस मांग की ईमानदारी पर भरोसा नहीं होता। चाहें तो सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर देख लें। क्या वक्त नहीं आ गया है कि सदस्यों की उपस्थिति को जरूरी किया जाए। कुछ देशों में ऐसे नियम हैं। अवरोध कम करने के लिए कुछ वर्षों से राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले शून्यकाल कर दिया गया है। इसका थोड़ा सकारात्मक असर दिखा है।
लोकसभा में भी इस पर विचार होना चाहिए। इसके भी ठोस नियम बनने चाहिए कि सप्ताह में चार दिन केवल सूचीबद्ध विषयों पर ही कार्यवाही चलेगी। आखिरकार सप्ताह के लिए बनने वाले एजेंडे में तो सभी बड़े दल शामिल होते ही हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं, जो सख्त नियम-कायदे को लोकतंत्र के ही खिलाफ बताएंगे, लेकिन संसदीय अराजकता और मनमानी को भी तो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। बात किसी दल की नहीं, सरकार और विपक्ष के मानसिकता की है। संसद को सही तरह चलना ही होगा।
कई विधानसभाएं ऐसी हैं, जो साल में 30 दिन भी नहीं चलती हैं, जबकि संविधान में अधिकतम छह महीने में सत्र बुलाने की बाध्यता है। कुछ समय पहले तक दिल्ली में तो विधानसभा को राजनीतिक मंच बना दिया गया था। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार कवच ओढ़कर मोदी सरकार पर मनचाहे आरोप लगाती थी, क्योंकि विधाई सदन में की गई टिप्पणियों पर कोर्ट में केस नहीं किए जा सकते। दो दिन के सत्र बुलाए जाते थे, फिर रोक दिए जाते थे। फिर इच्छा के अनुसार सत्र आहूत कर लिया जाता था। जिस विधाई सदन में बहुमत के लिए राजनीतिक दल कमर कसे खड़े होते हैं, उसे प्रासंगिक बनाने, सुचारू करने में किसी की रुचि नहीं दिखती।
सरकार के लिए विधेयक अहम हैं। कई बार तो यह सुविधाजनक भी होता है कि अवरोध में ही विधेयक पारित करा लिए जाएं, लेकिन सवाल विपक्ष का है कि वह सरकार के मुफीद ऐसा माहौल बनाता ही क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण होता है हर दो-तीन महीने में होने वाले चुनाव। ऐसे में सबको वही मुद्दे चाहिए, जो गर्मी पैदा कर सकें।
ब्रेकिंग न्यूज बना सकें। आरोप-प्रत्यारोप का मंच दे सके। क्या मान लेना चाहिए कि संसद तभी सुचारू ढंग से चल पाएगी और प्रासंगिक हो पाएगी, जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं? एक साथ चुनाव कई मर्ज की दवा साबित हो सकता है। तब गृहमंत्रालय के पास भी एनआरसी को पूरा करने का वक्त होगा और चुनाव आयोग के पास मौका होगा कि उसके आधार पर मतदाताओं की सूची दुरुस्त कर ले।
(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)



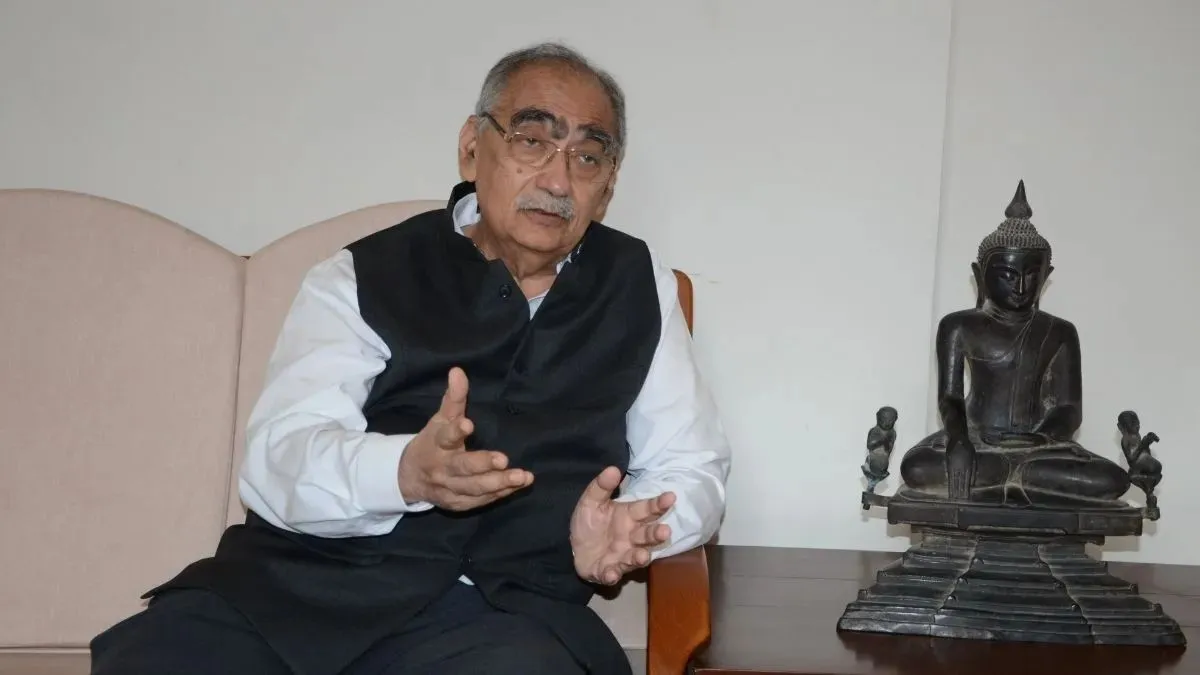










कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।