संपादकीय: लोकलुभावन वादों का पुलिंदा बनकर रह गए घोषणा पत्र, रेवड़ियां बांटने पर फोकस
चुनावों के दौरान दलों के घोषणा पत्र में लोगों की दिलचस्पी होती है, पर उनसे चुनाव जीतना मुश्किल है। घोषणा पत्र अब लुभावने वादों का पुलिंदा हैं, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं। कई राज्य सत्ता में आकर भी वादे पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। घोषणा पत्र कानूनी बाध्यता नहीं, इसलिए वादे पूरे करना भी अनिवार्य नहीं। अब ये मुफ्त चीजें बांटने जैसे हैं, जो विकास में बाधक हैं। जनता को चाहिए कि वे दलों से वादों को पूरा करने की क्षमता पर सवाल करें।
HighLights
घोषणा पत्र: लोकलुभावन वादों का पुलिंदा
वित्तीय स्थिति की अनदेखी
जनता की जागरूकता जरूरी
चुनावों के अवसर पर राजनीतिक दलों की ओर से जारी किए जाने वाले घोषणा पत्रों को लेकर उत्सुकता अवश्य रहती है, लेकिन यह कहना कठिन है कि चुनाव उन्हीं के जरिये जीते-हारे जाते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि घोषणा पत्रों में किए गए वादों के आधार पर किसी दल को जीत हासिल हुई हो।
इसका कारण यह है कि अब घोषणा पत्र लोकलुभावन वादों का पुलिंदा बनकर रह गए हैं। उनमें ऐसे तमाम आकर्षक वादे होते हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों के लिए पूरा करना संभव नहीं होता। हाल के समय में कई राज्यों में यह देखने को मिला है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के जिन वादों के साथ सत्ता में आए, उन्हें वे पूरा नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके, क्योंकि राज्य विशेष की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी।
कुछ राज्यों में तो यह भी देखने को मिला कि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के वादों को आधे-अधूरे ढंग से पूरा किया या फिर उन्हें पूरा करने की घोषणा करने के बाद ठिठक गए। जिस तरह घोषणा पत्र जारी करना कानूनी बाध्यता नहीं है, उसी तरह उनमें किए गए वादों को पूरा करना भी अनिवार्य नहीं है। इसका नतीजा यह है कि अब घोषणा पत्र रेवड़ियां बांटते दिखते हैं। यह ध्यान रहे कि रेवड़ियां वास्तविक विकास में बाधक ही बनती हैं।
बिहार में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्रों में अनेक ऐसे वादे हैं, जो कुल मिलाकर लोकलुभावन ही हैं। राजनीतिक दल घोषणा पत्रों में लोगों को लुभाने वाले तमाम वादे तो कर देते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते कि उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा? इसका एक कारण यह है कि आम जनता घोषणा पत्रों के वादों को लेकर ऐसे सवाल कभी नहीं पूछती कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य रखती है?
जिस दिन जनता यह जानने की कोशिश करने लगेगी, घोषणा पत्र गंभीरता के साथ तैयार किए जाने लगेंगे। जनता की ओर से राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे जनहित से जुड़े वास्तविक मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरें। दुर्भाग्य से ऐसा इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि वोट अभी भी जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या फिर रेवड़ियों के आधार पर पड़ते हैं।
इसी कारण योग्य प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाता और सुशासन स्थापित करना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता नहीं बन पाता। घोषणा पत्रों में किए गए वादों को लेकर परस्पर विरोधी दलों में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तो छिड़ता है, लेकिन उन्हें लेकर वैसी सार्थक बहस नहीं हो पाती, जैसी विकसित देशों में होती है और जिसके आधार पर वहां स्वस्थ जनमत तैयार करने में मदद मिलती है। हैरानी नहीं कि अपने यहां चुनावी घोषणा पत्र अपनी महत्ता खोते जा रहे हैं।






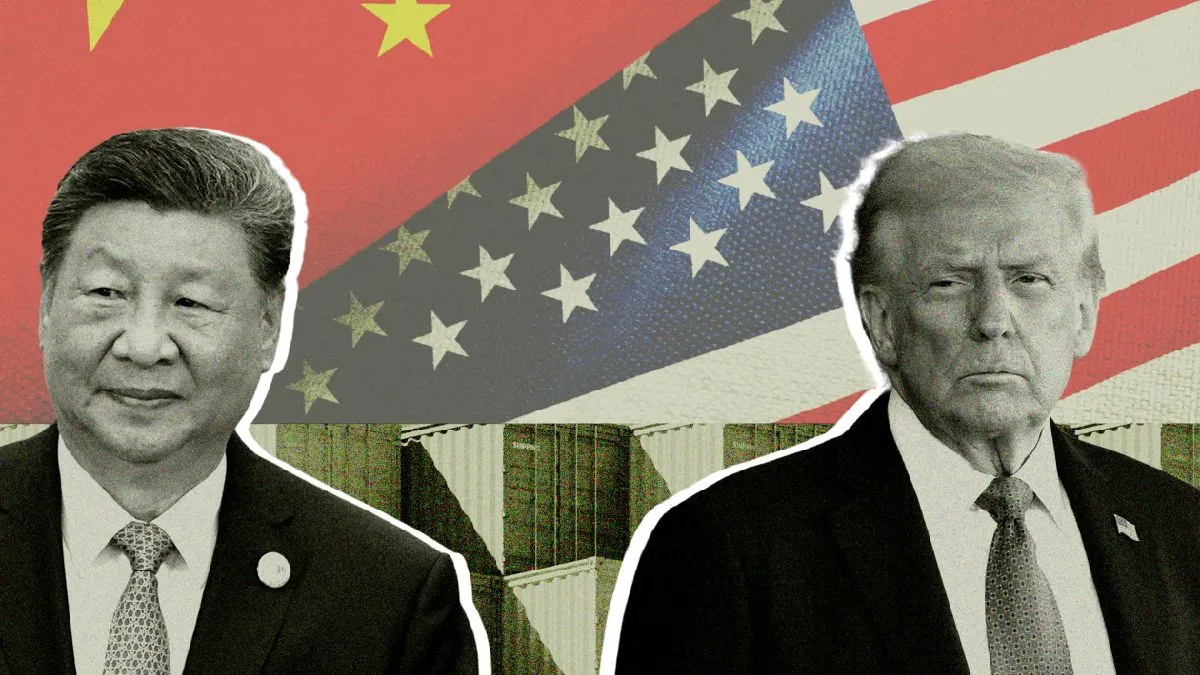





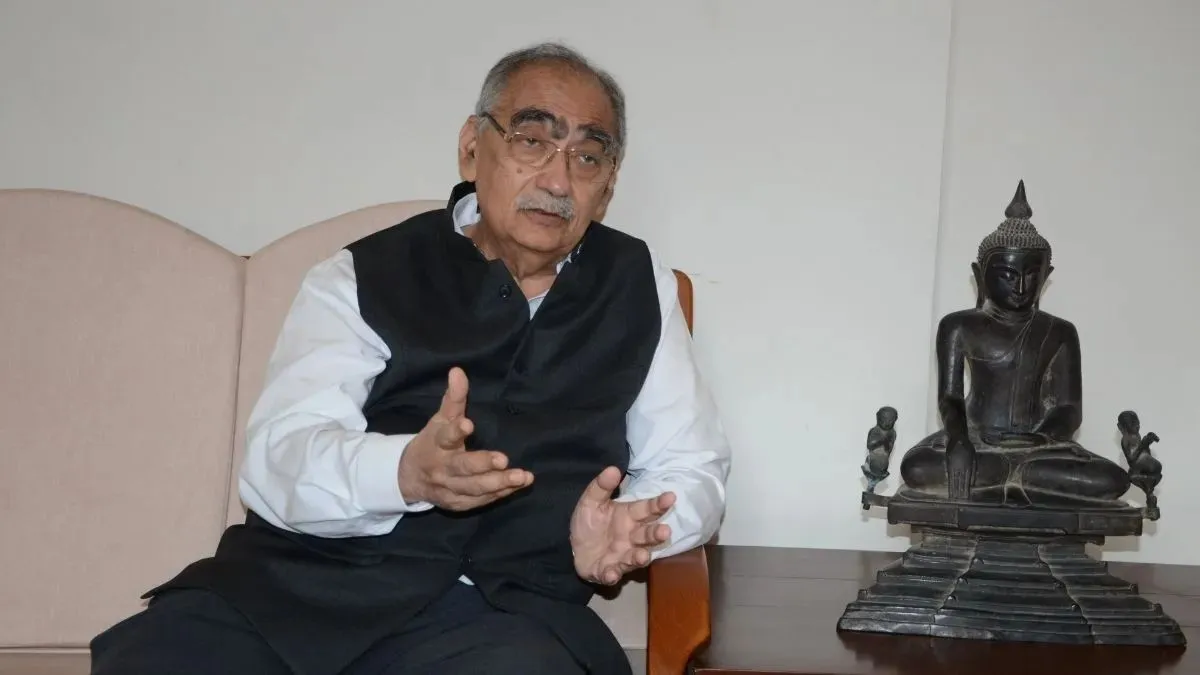
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।