विजयी बनने की आकांक्षा समाप्त कर देती है उचित-अनुचित की सीमा
साधनों की प्रचुरता के बावजूद अनेक लोग सुखी महसूस न करने पर आनंद की खोज में अन्यत्र भटकते हैं। कुछ लोग यश-कीर्ति में आनंद खोजते हैं।
नई दिल्ली (गणि राजेंद्र विजय)। दुख को जीवन का शाश्वत सत्य बताया गया है। सवाल यह है कि दुख का निवारण कैसे हो? इसकी खोज में अनंत काल से मनीषियों ने अपना जीवन अर्पित किया और पाया कि दुख का कारण है और इसका निवारण भी है। दुख के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है चाह, इच्छा या कामना। चाह का न होना और अनचाहे का हो जाना दुख का मूल कारण है। हम जन्म से ही कुछ न कुछ चाहते हैं और चाह की पूर्ति न होने पर हम दुखी होते हैं। दुख का दूसरा कारण है, हमारा शरीर जो रोगों का भंडार है। शरीर के धारण करते ही रोग व पीड़ा का जन्म हो जाता है। कई बच्चे तो जन्मते ही रोग के शिकार हो जाते हैं। कई रोगों पर तो नियंत्रण हो चुका है, परंतु अभी अनेक रोग लाइलाज हैं।
वृद्धावस्था में कुछ ज्यादा ही रोग उत्पन्न होते हैं। रोग से उत्पन्न पीड़ा व रोग के उपचार के खर्च से रोगी और परिजन दोनों दुखी रहते हैं। चाह का बदला रूप है आकांक्षा। हम जीवन में ऊंचा पद, यश और कीर्ति चाहते हैं। आकांक्षा प्रगति या विकास की जननी है, परंतु दुख का मूल भी है। आकांक्षा अपने आप में बुरी नहीं है, परंतु जब यह ममत्व व संग्रह की प्रवृत्ति से जुड़ जाती है तो यह न केवल स्वयं के लिए दुख का कारण बनती है, बल्कि पूरे समाज में विग्रह और विषमता का कारण भी बनती है।
आकांक्षा जन्म देती है अहं और लोभ को। अहं से पैदा होता है क्रोध और संघर्ष। विजयी बनने की आकांक्षा उचित-अनुचित की सीमा समाप्त कर देती है। संघर्ष जब हिंसात्मक हो जाता है तब मूक वर्ग (जिसमें गरीब समाज भी शामिल है) हिंसा के शिकार बनते हैं, भोग-उपभोग के साधन बनते हैं, शासित व दमित होते हैं। सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का आधार शोषण होने से व्यक्ति चाहकर भी शोषण के जाल से मुक्त नहीं हो पाता। जिनका साधनों पर कब्जा है, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं है, परंतु मजदूर और साधनहीन को तो सुबह होते ही मजदूरी पर जाना है।
साधनों की प्रचुरता के बावजूद अनेक लोग सुखी महसूस न करने पर आनंद की खोज में अन्यत्र भटकते हैं। कुछ लोग यश-कीर्ति में आनंद खोजते हैं। जो इसमें भी सुखी नहीं होते, वे अंतस की खोज प्रारंभ कर अध्यात्म में रमण करते हैं, परंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो अध्यात्म में सही जगह पर पहुंच जाएं।







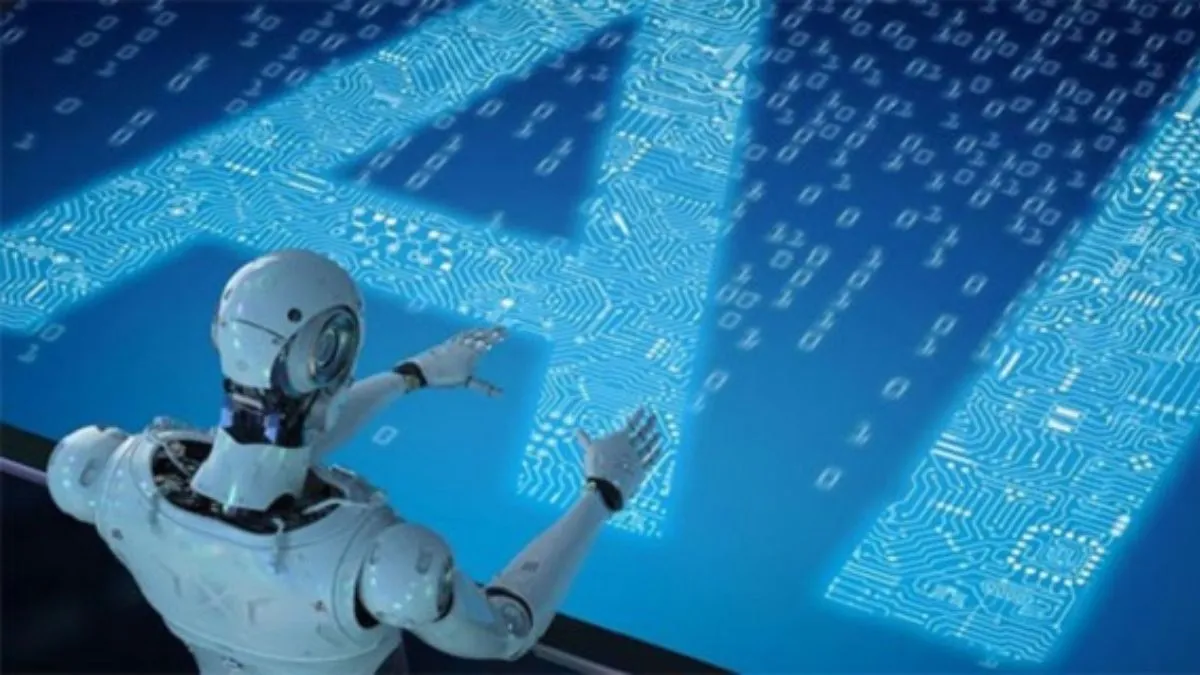






कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।