सोच बदलने का समय
किसी गांव की एक महिला बकरी खरीदना चाहती है। वह आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। यह जानते हुए कि उसे मदद मिल सकती है, वह इस काम के लिए लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआइ) में संपर्क करती है।
किसी गांव की एक महिला बकरी खरीदना चाहती है। वह आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। यह जानते हुए कि उसे मदद मिल सकती है, वह इस काम के लिए लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआइ) में संपर्क करती है। उसे लगभग 7,000 रुपये की जरूरत है। इतने पैसे किसी बैंक से तो उसे मिलेंगे नहीं। एक स्वयं सहायता समूह के जरिये काम कर रही एमएफआइ उसे 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज के हिसाब से यह ऋण देती है। उसे ये पैसे साप्ताहिक हिसाब से लौटाने हैं। इस ख्याल से यह ब्याज दर 36 फीसद होती है।
दूसरी तरफ उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल हैं। वह पंजाब सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम में बनने वाली बठिंडा पेट्रो रिफाइनरी में निवेश का फैसला करते हैं। पैसे के संकट से जूझ रही राज्य सरकार उन्हें पांच साल के लिए 0.1 फीसद ब्याज दर पर 1,250 करोड़ रुपये का ऋण देती है और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें 15 साल के टैक्स हॉलीडे (कर से मुक्ति) की सुविधा भी मिलती हैं। इसी तरह गुजरात में टाटा के नैनो कारखाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें 0.1 फीसद के ब्याज पर सैकड़ों करोड़ रुपये दिए थे। नि:संदेह उद्योग जगत की मदद के लिए हाथ बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि गांव की उस गरीब महिला को भी बकरी खरीदने के लिए 0.1 प्रतिशत की दर पर ऋण मिला होता तो वह साल के अंत में नैनो कार चला रही होती।
कुछ साल पहले मैंने कृषि खरीद और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रिपोर्ट पढ़ी थी। यह संस्था कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। खरीफ के मौसम से संबंधित इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि कपास के किसानों को बीस साल से अधिक समय तक जानबूझकर 20 फीसद कम कीमत दी गई ताकि टेक्सटाइल उद्योग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में, जो बात हम लोगों से कभी नहीं कही गई वह यह है कि यह वस्तुत: कपास किसान थे जो टेक्सटाइल उद्योग को इतने वर्षो तक सब्सिडी देते रहे हैं। कुछ महीने पहले कपास की कीमत साढ़े चार-पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। चूंकि इतने साल तक कपास के किसानों ने टेक्सटाइल उद्योग को सब्सिडी दी थी इसलिए मुङो उम्मीद थी कि संपन्न और शक्तिशाली टेक्सटाइल उद्योग ऐसे वक्त में कपास उगाने वालों की मदद के लिए आगे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों को अपना घाटा खुद भुगतना पड़ा।
ये दो उदाहरण बताते हैं कि ग्रामीण आबादी और मुख्यत: किसान किस तरह और कैसे पिछले वर्षो में आर्थिक रूप से कमजोर होते गए हैं। और यह सिर्फ कपास उत्पादकों का मसला नहीं है, हर तरह के किसानों को जानबूझकर उनकी फसल की कम कीमत दी जाती रही है ताकि उद्योगों को कच्चा माल कम कीमत पर मिलता रहे या उन्हें इसलिए दंडित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं तक कम कीमत में सामान पहुंचाया जा सके। मैं कभी नहीं समझ पाया कि सिर्फ किसान ही उपभोक्ताओं तक सामान कम कीमत में पहुंचाने के लिए क्यों भुगतें? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि दुनिया भर में कृषि उत्पादों के मूल्य सभी उत्पादों के लिए समान रहे हैं। अगर आप मुद्रास्फीति के नजरिये से देखें तो किसान 2015 में गेहूं और चावल के लिए जो कीमत पा रहा है वह उतनी ही है जितनी 1995 में थी।
2014 की नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट हमें बताती है कि एक किसान परिवार की अपनी कृषि गतिविधियों से औसत मासिक आय मामूली 3,078 रुपये है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक किसान परिवार को मनरेगा समेत कुछ अन्य गैर कृषि कार्य करने पड़ते हैं। तब उसे 6,000 रुपये प्रति परिवार प्रति महीने हासिल होते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि 58 फीसद किसान भूखे पेट सोते हैं और मौका मिले तो 76 फीसद किसानी छोड़ना चाहते हैं। अगर किसानों को अपने उत्पाद की सिर्फ पूरी कीमत दे दी जाती तो कृषि संकट इतना गहरा नहीं होता।
मई, 2014 में राजग सरकार के आने के बाद इस साल गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। पिछले साल गेहूं किसानों को 1,400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला, इस साल उन्हें 1,450 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जो 3.2 फीसद अधिक है। दूसरी तरफ, सरकारी कर्मचारियों को इसी अवधि में डीए की दो किस्तें दी गई हैं, जो उनके वेतन का 13 फीसदी है। किसानों के लिए कम कीमत सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन यही सिद्धांत तब नहीं अपनाया जाता जब मसला सरकारी कर्मचारियों का हो। वे तो सामान्य ढंग से डीए पाते रहते हैं। फिर वही बात, ये किसान हैं जो उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे हैं। मुख्य रूप से यही कारण है कि कृषि घाटे का सौदा होती जा रही है। योजनाकार और नीति नियंता इसीलिए किसानों को शिक्षा से विमुख रखना चाहते हैं।
किसानों के लिए बेहतर आर्थिक भविष्य के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण को न्यायोचित ठहराया जा रहा है। मैंने वित्तमंत्री को यह कहते हुए कई मर्तबा सुना है कि वे उद्योगों का सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उद्योगों से मिलने वाले राजस्व का वह ग्रामीण इलाकों में निवेश करना चाहते हैं। 2004-05 से पिछले दस साल में उद्योगों को 42 लाख करोड़ रुपये की टैक्स छूट दी गई है ताकि औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन बढ़ सके तथा रोजगार में वृद्धि हो। लेकिन इस तरह कुछ हुआ तो है नहीं। यह आड़ी-तिरछी आर्थिक सोच इस तरह की नीतियां बना रही हैं जो किसानों को किसानी छोड़कर शहरों की तरफ धकेल रही है। अनुमान है कि अगले करीब 15 साल में यानी 2030 तक भारत की आबादी के लगभग 50 फीसद लोग शहरी इलाकों में रहने लगेंगे। ये शहर और नगर भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2 फीसद हिस्से को घेर लेंगे। मेरे विचार से यह न सिर्फ आर्थिक पागलपन है, बल्कि राजनीतिक और वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव भी दिखाता है। आबादी के इतने भारी पलायन से होगा यह कि शहरों में रहना अविकसित बस्तियों में रहने जैसा होगा। पहले ही मुंबई की आबादी के 60 प्रतिशत लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इसलिए, आर्थिक दृष्टि बदलनी होगी।
किसान भी उद्यमशील हैं और गांवों में रहने वाली युवा पीढ़ी भी शुरुआत कर सकती है। उन्हें सिर्फ योजनाओं के समर्थन की जरूरत है। यह गांवों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के जरिये किया जाना चाहिए। अब तक देहात को संसाधनों के अभाव के साथ रखा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 60 करोड़ लोगों के आश्रित होने के मद्देनजर यह चना-चबेना जैसा है।
(देविंदर शर्मा-लेखक खाद्य एवं कृषि नीतियों के विश्लेषक हैं)



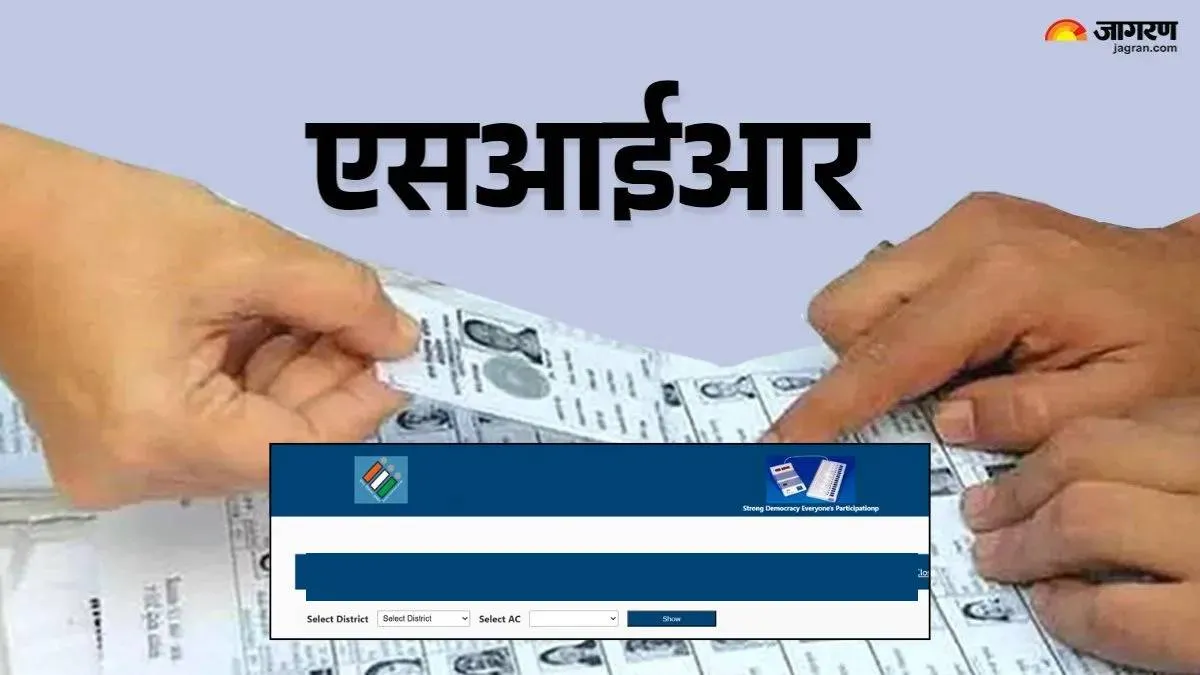










कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।