हवा में एक फीसदी PM2.5 बढ़ने से 9.6% बढ़ जाते हैं डिप्रेशन के मामले, बच्चों के मानसिक विकास पर भी असर
शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अध्ययनों के अनुसार, हवा में पीएम2.5 की मात्रा में एक फीसदी की वृद्धि होने से डिप्रेशन के मामले 9.6% तक बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे संज्ञानात्मक विकास धीमा हो सकता है। वायु प्रदूषण से श्वसन और हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं।

नई दिल्ली, विवेक तिवारी। भारत में बढ़ता वायु-प्रदूषण अब सिर्फ फेफड़ों और दिल के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार, हवा में PM2.5 के स्तर में सिर्फ एक माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी मानसिक बीमारियों के मामलों में तेज़ इजाफा करती है। इस मामूली बढ़ोतरी से हर एक लाख लोगों में डिप्रेशन के 9.6%, एंज़ाइटी के 5.3% और तनाव से जुड़ी परेशानियों के 2.6% नए मामले सामने आते हैं। सिर्फ बाहर की हवा ही नहीं, घर के अंदर की हवा भी बच्चों के दिमाग के लिए उतनी ही हानिकारक साबित हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया (UEA) के शोध में पाया गया कि भारत की इनडोर वायु गुणवत्ता दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बाधित कर रही है। UEA के प्रमुख शोधकर्ता जॉन स्पेंसर के अनुसार, ग्रामीण भारत के घरों में PM2.5 की अधिकता से न सिर्फ बच्चों की सीखने-समझने की क्षमता घटती है, बल्कि भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में पहले से ही PM2.5 का औसत स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सीमा से 5 से 10 गुना अधिक है, और हर साल यह खतरा और भी गहराता जा रहा है।
लीड्स विश्वविद्यालय के पृथ्वी एवं पर्यावरण स्कूल के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, 2050 तक भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ा संकट बन जाएगा। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। सर्दियां शुरू होते ही देश के कई शहर गंभीर वायु प्रदूषण के संकट से जूझने लगते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 16 लाख लोगों की मौत होती है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारतीयों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते 2050 तक हवा में इसकी मात्रा दोगुनी तक बढ़ सकती है। इससे एक गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है।
दिल्ली में हर साल सर्दियां शुरू होने से पहले गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या देखने में आती है। प्रदूषण बढ़ते ही डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मामले भी बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के प्रोफेसर एवं मनोचिकित्सक डॉ. ओम प्रकाश कहते हैं कि, जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो लोग आमतौर पर सांस की बीमारी या फेफड़ों के नुकसान के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रदूषण मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। प्रदूषण के महीन कण शरीर में सूजन पैदा करते हैं और यह सूजन मस्तिष्क तक पहुँचकर मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। इससे अवसाद, चिंता, नींद की गड़बड़ी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। कई बार लोग तनाव और उदासी के पीछे केवल व्यक्तिगत कारण खोजते हैं, जबकि प्रदूषित वातावरण भी एक बड़ा कारण हो सकता है।
हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा बच्चे और बुज़ुर्ग लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। बुज़ुर्गों में पहले से मौजूद अवसाद या डिमेंशिया के लक्षण बढ़ सकते हैं। मानसिक रोग से पीड़ित लोगों में बेचैनी और नींद की समस्या अधिक हो सकती है। प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए लोगों को सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए। ये मास्क PM2.5 जैसे कणों को रोक देता है। ये प्रदूषक कण मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं। मास्क लगाने से कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण से भी बचाव होता है।
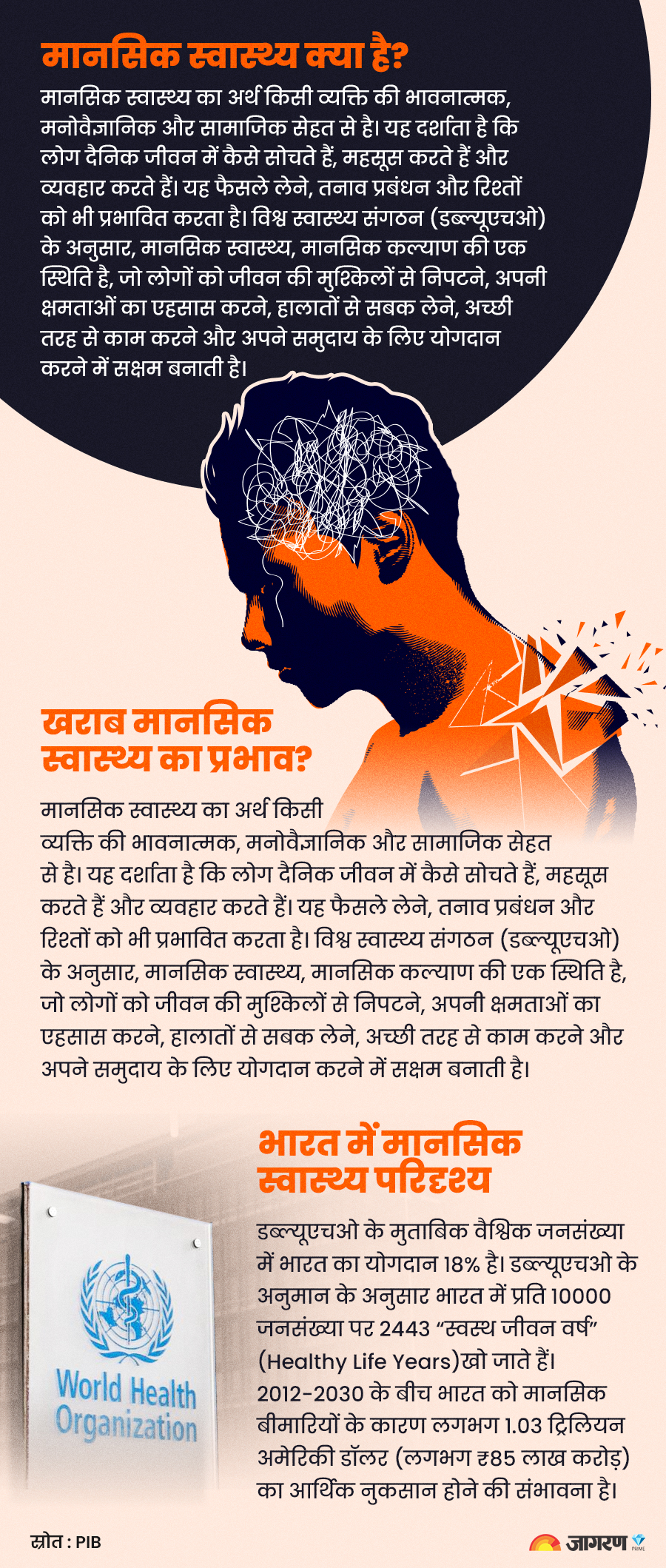
लैंनसेट में छपे एक अध्ययन में सामने आया है कि बढ़ता वायु प्रदूषण धूम्रपान की तरह ही ब्रेन स्ट्रोक का बड़ा कारण बन रहा है। प्रदूषित वायु में ज्यादा समय तक रहने से मस्तिष्क और इसे ढकने वाले ऊतकों के बीच रक्त वाहिकाएँ फट जाती हैं। इससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में लैंनसेट में छपे एक अध्ययन के मुताबिक 1990 और 2021 के बीच, दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में 70 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 44 फीसदी तक बढ़ी है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि 2021 में स्ट्रोक के 84% मामलों में ब्रेन स्ट्रोक का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण, ज्यादा शारीरिक वजन, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान और नियमित व्यायाम न करना है। ऐसे में इन बातों का ध्यान रख ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में काफी कमी लाई जा सकती है।
अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन में मुख्य शोध वैज्ञानिक और इस शोध की सह-लेखक डॉ. कैथरीन ओ. जॉनसन के मुताबिक, "एशिया और अफ्रीका के कई देशों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। बढ़ती गर्मी, वायु प्रदूषण, लोगों में बढ़ता मधुमेय, ब्ल्ड प्रेशर ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को और बढ़ा रहा है। ऐसे में इन देशों की युवा आबादी में आने वाले समय में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा और बढ़ने की संभावना है। 2021 में, स्ट्रोक के लिए पांच प्रमुख वैश्विक जोखिम कारक उच्च सिस्टोलिक रक्तचाप, पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण, धूम्रपान और उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहे। इनमें आयु, लिंग और स्थान के अनुसार काफी भिन्नता भी देखी गई।
इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की जनरल सब कमेटी के अध्यक्ष और प्रोफेसर एवं मनोचिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि वायु प्रदूषण मां की कोख से ही बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है। अगर कोई गर्भवती महिला किसी बेहद वायु प्रदूषित जगह पर रहती है तो संभव है कि उसके बच्चे के दिमाग के विकास पर असर पड़े। यहां तक ही कई मामले में हमने देखा है कि ध्वनि प्रदूषण से भी बच्चों के दिमाग के विकास पर असर पड़ता है। पहले हम मानते थे कि दो साल में बच्चों का दिमाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। लेकिन कई अध्ययनों में सामने आया है कि दिमाग का विकास दो साल के बाद भी होता रहता है। वायु प्रदूषण की स्थिति में हवा में मौजूद लेड और PM10 और PM2.5 जैसे कण बच्चों के दिमाग के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
हवा में प्रदूषण का स्तर खास तौर पर पर्टिकुलेटेड मैटर बढ़ने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे गुस्सा भी ज्यादा आता है। सबसे अधिक मुश्किल तब होता है जब हवा प्रदूषण ज्यादा होने पर व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। बाहर कम निकलने या घर में ज्यादा देर तक फोन या किसी अन्य स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से दिमाग में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में नींद न आने या बार बार नींद टूटने की समस्या होती है। वहीं व्यक्ति का टॉलरेंस लेवल भी कम हो जाता है और उसे बहुत जल्द गुस्सा आने लगता है। लम्बे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने पर डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में हवा में प्रदूषण बढ़ने पर भी व्यक्ति को शारीरिक तौर पर सक्रिय रहना जरूरी है। भले बाहर कम निकलें पर घर पर एक्सरसाइज जरूर करें। थोड़े समय के लिए ही सही बाहर निकलें। ध्यान रहे मास्क जरूर लगा लें
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सबअरेक्नॉइड रक्तस्राव के लिए एक बड़ा खतरा है। ये ब्रेन स्ट्रोक के इस प्रकार के कारण होने वाली मृत्यु और विकलांगता में 14% का योगदान देता है, जो धूम्रपान से होने वाले ब्रेन स्ट्रोक के मामलों के बाराबर है। वायु प्रदूषण कई तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लखनऊ स्थिति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी कहते हैं कि, हवा में प्रदूषण के दौरान कई ऐसे केमिकल होते हैं तो दिगाम में न्यूरो इंफ्लेमेशन के खतरे को बढ़ाते हैं। वहीं हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर नसों और धमनियों में फैट जमा करता है, जिससे खून के प्रवाह में बाधा पहुंचती है। ब्रेन स्ट्रोक के कारणों को प्रमुख रूप से दो तरह से बांटा जाता है। एक, धूम्रपान न करके, वायु प्रदूषण से दूर रहके, वजन को नियंत्रित करके, ज्यादा तनाव न लेकर और निमयित व्यायाम कर खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं दूसरे ऐसे कारण हैं जिन्हें कम नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण एशिया के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा दुनिया के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। किसी व्यक्ति में जैनेटिक हिस्ट्री को तो उसे खतरा बना रहता है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। वहीं हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि साफ हवा में रहने वाले या गांवों में रहने वाले लोगों की तुलना में शहरों में या प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोगों को डिमेंशिया का खतरा आठ से दस गुना तक ज्यादा होता है।
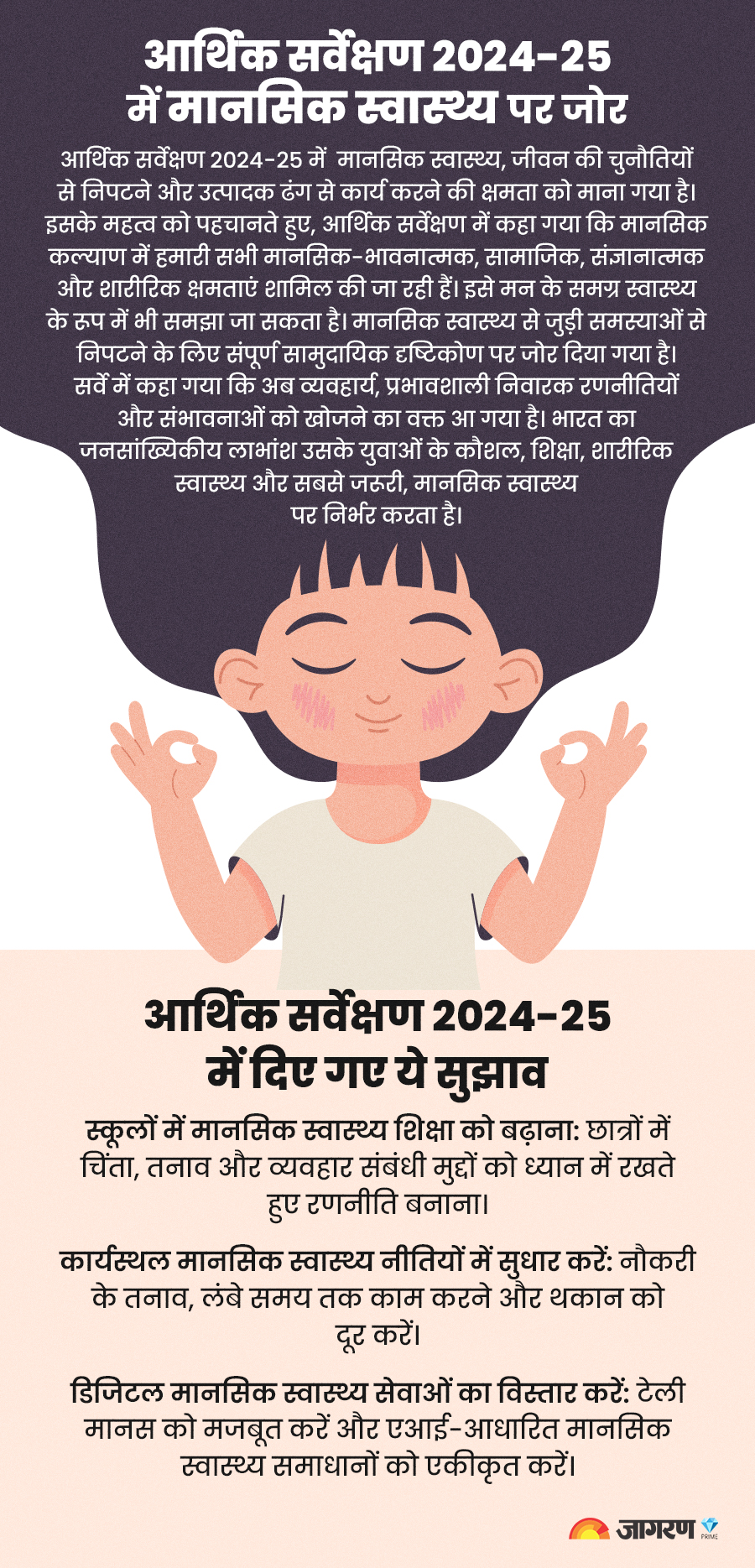
भारत सरकार लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं पर काम कर रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, साल 2024 में, मानसिक स्वास्थ्य में अधिक पोस्टग्रेजुएट छात्रों को प्रशिक्षित करने और बेहतर इलाज उपलब्ध करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य में 47 पीजी विभाग स्थापित या अपग्रेड किए गए हैं। 22 नए बनाए गए एम्स में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जा रही हैं। 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची, सहित सरकार लगभग 47 और मानसिक अस्पताल चला रही है। आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत, सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सेवाओं के पैकेज में, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।