अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करती रेवड़ी संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है ऐसी राजनीति
Revdi Culture in Politics मुफ्तखोरी की राजनीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली भी है। पढ़ें दैनिक जागरण अखबार के प्रधान संपादक संजय गुप्त का लेख ...
[संजय गुप्त]। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले कुछ दिनों में दो बार देश का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुके हैं कि रेवड़ी संस्कृति किस तरह लोकतंत्र और अर्थतंत्र का बेड़ा गर्क कर रही है। यह वही संस्कृति है, जिसे मुफ्तखोरी की राजनीति भी कहा जाता है। यह राजनीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि रेवडिय़ां बांटने की राजनीतिक संस्कृति ने न जाने कितने देशों को तबाह किया है।
यूरोप भुगत चुका है खामियाजा
यूरोप के कुछ विकसित देश इसी रेवड़ी संस्कृति के कारण आज आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भारत के पड़ोस में ही श्रीलंका, पाकिस्तान का भी इसी रेवड़ी संस्कृति ने बुरा हाल किया है। अपने देश में ही देखा जाए तो कई राज्य सरकारें इस रेवड़ी संस्कृति के कारण लगभग दीवालिया होने की कगार पर हैं। उनका बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे मुफ्तखोरी की राजनीति का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं। इस राजनीति ने राज्य के बिजली बोर्डों का भी बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि राज्य सरकारें चुनावी लाभ के लिए मुफ्त में या लागत से बहुत कम में बिजली दे रही हैं। इसका दुष्परिणाम बिजली बोर्ड भुगत रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई
यह अच्छा है कि उच्चतम न्यायालय उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें रेवड़ी संस्कृति पर लगाम लगाने की मांग की गई है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि मुफ्तखोरी की राजनीति देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने इस विषय को गंभीर मानते हुए एक ऐसी समिति बनाने का सुझाव दिया, जिसमें केंद्र सरकार, चुनाव आयोग के साथ नीति आयोग, रिजर्व बैंक और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हों।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा उठा चुके हैं सवाल
उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जब सांसद एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि इस पर उनकी क्या राय है तो उन्होंने इस मामले से चुनाव आयोग को बाहर रखने की बात कही। स्वाभाविक रूप से सालिसिटर जनरल उनकी राय से सहमत नहीं हुए। इसी अवसर पर जब किसी ने यह सुझाव दिया कि इस विषय पर संसद में बहस होनी चाहिए तो मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने सवाल किया कि आखिर इस पर कौन राजनीतिक दल गंभीरता से बहस करेगा?
राजनीतिक दलों की मंशा पर सवाल
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा का यह सवाल सही है, क्योंकि जब करीब-करीब सभी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हों, तब फिर वे संसद में इस पर कोई सार्थक बहस कैसे कर सकते हैं? हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि कई राजनीतिक दल तरह-तरह के तर्कों से रेवड़ी संस्कृति का न केवल बचाव कर रहे हैं, बल्कि उसे जरूरी भी मान रहे हैं।
चुनाव आयोग को अधिकार मिले तब तो बने बात
वास्तव में इसी कारण मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी दल रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ बात करने वाला नहीं है। नि:संदेह इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन तभी जब उसे पर्याप्त अधिकार मिलें और वह राजनीतिक दलों की मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली मनमानी घोषणाओं पर अंकुश लगाने में सक्षम हो।
रेवड़ी संस्कृति से होने वाले नुकसान को समझें
अभी तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर ही अपनी आपत्ति जता सकता है। वह चुनाव बाद बनी सरकार की ओर से लिए जाने वाले लोकलुभावन फैसलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में बात तब बनेगी, जब सभी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति से होने वाले नुकसान को समझें और उस पर स्वत: ही अंकुश लगाएं, लेकिन ऐसा होने के आसार नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ दल तो अनाप-शनाप लोकलुभावन घोषणाएं करके एक तरह से वोट खरीदने लगे हैं। यह ठीक है कि औसत मतदाता परिपक्व हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं जो मुफ्त की योजनाओं से होने वाले नुकसान को समझ सकें।
रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक
जैसे यह एक तथ्य है कि रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, वैसे ही यह भी कि देश में एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है और उसे कई तरह की राहत और रियायत देने की आवश्यकता है। इस जनसंख्या को गरीबी रेखा से निकालने के लिए किसी न किसी रूप में सब्सिडी यानी सरकारी राहत देनी ही होगी, लेकिन इसके लिए कोई पैमाना बनना चाहिए, जैसा कि आरक्षण के मामले में बना है।
बने नियम
इसी के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं और लोकलुभावन योजनाओं के बीच के अंतर को भी परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई नियम भी बनना चाहिए कि बजट का कितना प्रतिशत धन जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है?
गरीबों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो रहा सुधार
यह नियम सभी राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी होना चाहिए-वह चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल। जो भी वित्तीय सहायता अथवा सुविधा या सामग्री गरीबों को दी जाए, उसका लेखा-जोखा भी रखा जाना चाहिए और संबंधित योजनाओं की समीक्षा भी होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि उनसे अपेक्षित लाभ हो रहा है या नहीं? यदि किसी लोकलुभावन योजना से गरीबों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार न हो रहा हो और उनका जीवन स्तर ऊपर न उठ रहा हो तो फिर उसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं।
आम जनता को भी चेतना चाहिए
चुनाव जीतने के इरादे से राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं को लेकर आम जनता को भी चेतना चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाएं अंतत: उसके लिए मुसीबत बनती हैं और अर्थव्यवस्था का बेड़ा भी गर्क करती हैैं। मनरेगा योजना के बारे में रह-रहकर यह सवाल उठता रहता है कि आखिर यह कानून लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में कितनी सहायक है? इसी तरह यह सवाल भी उठता रहता है कि कर्ज माफी की योजनाएं किसानों और कृषि का कितना भला कर पा रही हैं?
वोट हासिल करने के लिए कर्ज माफी करने की घोषणाएं
यह निराशाजनक है कि कर्ज माफी योजनाओं की नाकामी के बावजूद कई राजनीतिक दल चुनाव के मौके पर खुद को किसानों का हितैषी साबित करने और उनके वोट हासिल करने के लिए कर्ज माफी करने की घोषणाएं करते रहते हैं। यह ठीक नहीं। जनकल्याण की योजनाओं के मामले में यह भी देखा जाना चाहिए कि उनका लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले। यदि जनकल्याण की आड़ में की जाने वाली मुफ्तखोरी की राजनीति लोगों को बैसाखी प्रदान करने या फिर उन्हें काम न करने के लिए प्रेरित करे तो फिर ऐसे लोग न तो कभी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और न ही देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।
.jpg)
[लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं]









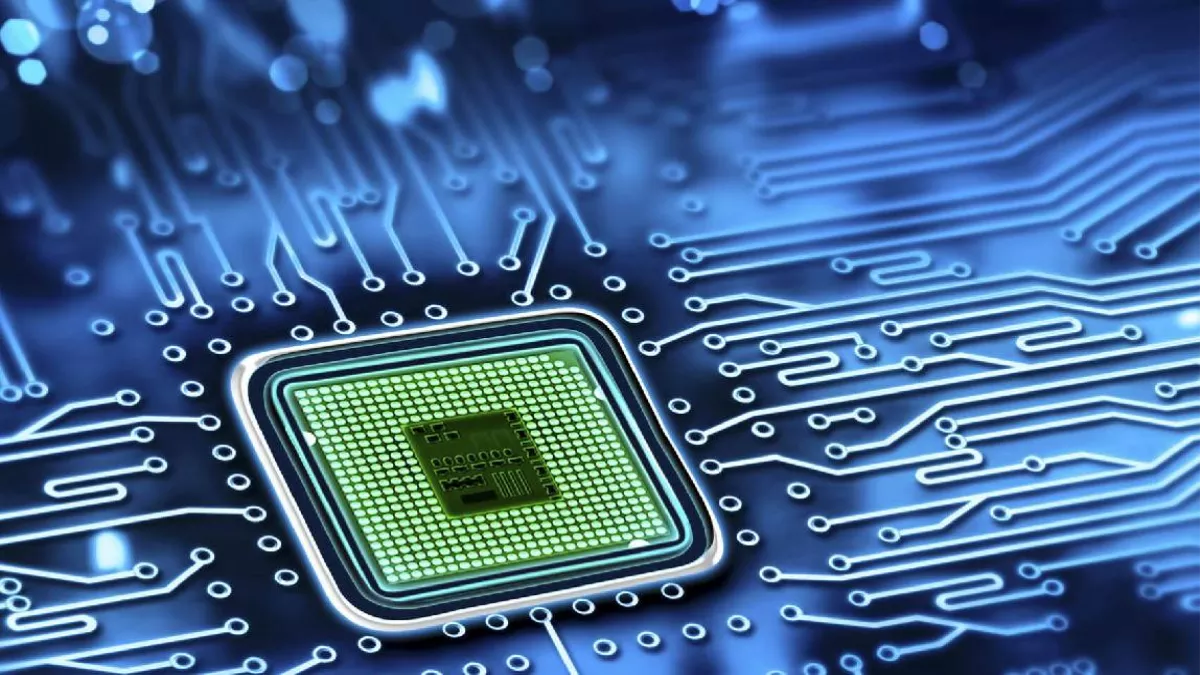




कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।